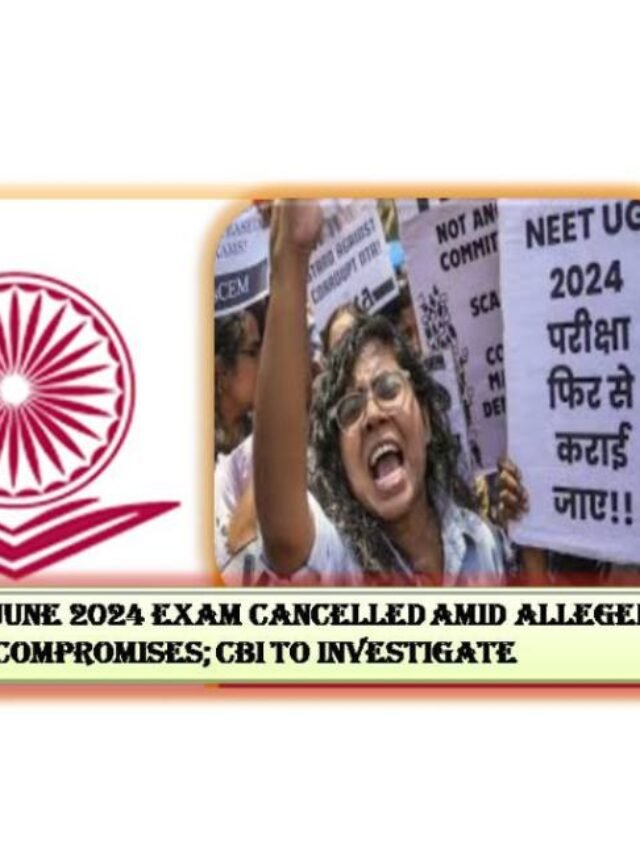भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर चर्चा करें: – संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।”
राज्य शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 21 में नहीं किया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 21 राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्ति पर भी लागू होता है। हालाँकि अनुच्छेद मुख्य रूप से राज्य पर केंद्रित है और राज्य के निम्नलिखित कर्तव्य हैं: –
यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम नहीं करेगा। कानून बनाकर राज्य यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि निजी व्यक्ति भी दूसरों के व्यक्तिगत का उल्लंघन नहीं करता है।
कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो स्वयं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं। उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करना राज्य का कर्तव्य है। यहां यह कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति या समूह के जीवन की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण के लिए सामाजिक न्याय लाने के लिए राज्य का कर्तव्य है और इसलिए सामाजिक न्याय अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के बीच एक अतिव्यापी है। व्यक्ति और समूह के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गरिमा की रक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक भेदभाव और उत्थान की अवधारणा भी अनुच्छेद 21 में निहित है, लेकिन कला के संदर्भ में इसका खुलासा नहीं किया गया है। 21 जैसा कि समानता और सामाजिक न्याय U/A 14 के संदर्भ में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।
अमेरिकी संविधान के संदर्भ में नियत प्रक्रिया
अमेरिकी संविधान के संदर्भ में नियत प्रक्रिया की अवधारणा का अर्थ है कि भारतीय संविधान में राज्य के तीन अंगों के बीच निर्धारित किया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में नियत प्रक्रिया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, हालांकि के.एन. बुनियादी ढांचे का भारती निर्णय
इस बोध का सिद्धांत है कि समानता, न्याय की तर्कसंगतता और गैर-मनमानापन के सिद्धांत संविधान के आवश्यक सिद्धांत हैं। यह भी महसूस किया गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना कोई और हर प्रक्रिया नहीं हो सकती है।
अनुच्छेद 21 से संबंधित केस कानून – किस हद तक ARTICLE 21/अनुच्छेद 21 लागू
व्यक्तिगत स्वतंत्रता
ए.के. गोपालन बनाम भारत संघ (A.I.R-1950)
सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह माना कि कला 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब और कुछ नहीं है भौतिक शरीर की स्वतंत्रता की तुलना में, जो कि कानून के अधिकार के बिना निरोध और गिरफ्तारी से मुक्ति है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘राज्य निर्मित कानून’ के रूप में कानून की व्याख्या/व्याख्या की।
“कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” या कानून की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग:- ए.के. गोपालन बनाम भारत संघ (A.I.R-1950)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कला 21 के तहत इस्तेमाल किया गया शब्द कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। यदि किसी कानून द्वारा कोई प्रक्रिया स्थापित की गई है और उस प्रक्रिया का उपयोग करके किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया गया है। इसलिए इसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह उचित है या नहीं।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (A.I.R 1978)
इस मामले में यदि अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। यह नहीं कहा जा सकता कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संवैधानिक है।
मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (A.I.R 1978)
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीने का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
आजीविका का अधिकार
वेलो सिटिजन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (A.I.R 1996)
यह माना गया कि राज्य देश के सभी संसाधनों का सार्वजनिक ट्रस्ट है और लोग उस सार्वजनिक ट्रस्ट के लाभार्थी हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संसाधनों का इस प्रकार प्रबंधन करे कि वह लोगों के हित में सर्वोत्तम ढंग से कार्य करे। इन संसाधनों के प्रबंधन के मामले में राज्य लोगों के प्रति जवाबदेह है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों (अर्थात लाभार्थी) के हित में पर्यावरण के संरक्षण के प्रयास करें।
चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (A.I.R-1996)
यह माना गया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, पानी, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, संस्था के सभ्य वातावरण के लिए बुनियादी और सुविधाओं का अधिकार है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को ये बुनियादी सुविधाएं और आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करे।
स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार
परमानंद कटारा (पी.के) बनाम भारत संघ (यू.ओ.आई) 1989 S.C
यह माना गया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा उपचार का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दुर्घटना या किसी गंभीर चोट के मामले में पुलिस कार्यवाही के लिए डॉक्टरों का कर्तव्य है।
मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार
महाराष्ट्र राज्य बनाम मनु भाई प्रग्गी वाशी 1995 S.C.
यह माना गया कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना राज्य का कर्तव्य है।
प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघ (A.I.R 1995 S.C.)
यह माना गया कि सम्मानजनक जीवन के अधिकार में अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है जो अपने आप में है
प्रदूषण मुक्त/गैर प्रदूषणकारी पर्यावरण का अधिकार शामिल है।
मुरली एस. देवरिया बनाम भारत संघ (A.I.R 2002 S.C.)
यह माना गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान दूसरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए
गरिमा का अधिकार
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (A.I.R 1997 S.C.)
गरिमा का अधिकार विशेष रूप से यौन गरिमा हर महिला का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश तय किए थे। महिला सुरक्षा और गरिमा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित है।
बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ए.आई.आर 2011 S.C)
यहां तक कि यौनकर्मियों को भी गरिमापूर्ण जीवन और जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है। उन्हें अपने पेशेवर जीवन जीने और समाज की मुख्य धारा में आने का अधिकार है। इस मामले में अदालत ने यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया और सिफारिश की कि राज्य को बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उचित कानून बनाना चाहिए ताकि वे अपने लिए आजीविका अर्जित कर सकें।
एकान्तता का अधिकार
अमर सिंह बनाम भारत संघ ए.आई.आर 2011 S.C
यह माना गया था कि अनुच्छेद 21 ने अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति की निजता के अधिकार को निहित किया है। टेलीग्राफ अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही के बिना कोई भी टेलीफोन ट्रैकिंग अवैध होगी और प्रभावित व्यक्ति उस सेवा प्रदाता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है जिसने उस विशेष टैपिंग की अनुमति दी थी। (कानून द्वारा प्रक्रिया को छोड़कर शामिल नहीं है)
शीघ्र परीक्षण का अधिकार
हुसैनारा खातो बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (ए.आई.आर 1979)
अदालत ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार आरोपी को सभी चरणों में उपलब्ध है, जैसे कि जांच, जांच, परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विचार।
हथकड़ी लगाने का अधिकार
प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासनिक (ए.आई.आर. 1980)
अदालत ने कहा कि यह कैदियों का मौलिक अधिकार है कि जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो, उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी।
क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है?- अब चर्चा करते हैं: –
पी.राथिनम बनाम भारत संघ में, प्रश्न उठता है कि क्या आईपीसी की धारा 309 संवैधानिक है या नहीं?
- अदालत ने माना कि संविधान में गारंटीकृत किसी भी सकारात्मक अधिकार में नकारात्मक अधिकार भी शामिल है और इसलिए जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल होगा।
- अदालत ने माना कि आईपीसी को मानवीय बनाने की जरूरत है। एक व्यक्ति जो पहले से ही पीड़ित है और उस मनःस्थिति में वह खुद को मारने का प्रयास करता है, उसे इस तरह के आत्महत्या के प्रयास के लिए दंडित करके और अधिक पीड़ित नहीं किया जा सकता है।
जियान(GIAN KAUR) कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में, एस.सी
- इस मामले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि आईपीसी की धारा 306 संविधान में है, पांच जजों की बेंच ने जे.एस वर्मा का फैसला सुनाया,
यह माना गया कि जीवन का अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं है बल्कि यह सही है कि किस हद तक। यह कार्रवाई की स्वतंत्रता के रूप में नहीं है बल्कि यह अपने अस्तित्व के अधिकार के रूप में है जो व्याख्या कला के संबंध में लागू की गई है। 19(1)(ए) Article के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है।
- यदि मरने के अधिकार की अनुमति दी जाती है तो इससे गंभीर सामाजिक प्रभाव पड़ेगा कि यह आत्मघाती अलार्म पैदा करेगा। लोगों के बीच और सामाजिक अंतरात्मा की खातिर। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी भी समस्या पर आत्महत्या कर सकता है जो समाज के लिए हानिकारक होगा।
- धारा 309 I.P.C आत्महत्या के मामलों में समाज पर एक निवारक भूमिका निभाता है।
- पी.रतिनम का फैसला गलत तरीके से तय किया गया था, न तो आईपीसी की धारा 309 और न ही आईपीसी की धारा 306 असंवैधानिक है।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु या दया हत्या से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय।
अरुणा रामचंद्र शनभाग बनाम भारत संघ 2011, S.C
इच्छामृत्यु दो प्रकार की होती है सक्रिय इच्छामृत्यु और निष्क्रिय इच्छामृत्यु।
S.C ने माना कि भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु पूरी तरह से अवैध है।
और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के संबंध में अदालत ने माना कि यह मान्य है यदि प्रदान की गई निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: –
- माता-पिता या पति या पत्नी या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार या पीड़ित का कोई दोस्त या पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करना होगा जो आवेदक की वास्तविकता की जांच करेगा और वह उच्च न्यायालय के दो मौजूदा न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त करेगा।
- समिति उस क्षेत्र के 3 प्रतिष्ठित डॉक्टरों से परामर्श करेगी और केवल ऐसे डॉक्टरों की राय पर जो टीम का हिस्सा हैं और उचित जांच के बाद ही समिति दया हत्या की अनुमति देगी. डॉक्टरों की राय है कि पीड़ित के बचने की कोई संभावना नहीं है और पीड़ित बेवजह पीड़ित है।
इसका मतलब है कि भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु पूरी तरह से अमान्य है और यदि प्रदान की गई शर्तों को पूरा किया जाएगा तो निष्क्रिय इच्छामृत्यु मान्य है।